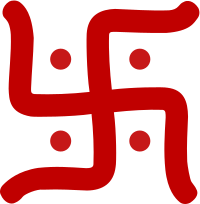वैदिक धर्म
वैदिक धर्म, वैदिक वर्णाश्रम वैदिक सभ्यता का मूल था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में हज़ारों वर्षोंपूर्व से है।

|
हिन्दू धर्म |
 |
| इतिहास · देवता |
| सम्प्रदाय · पूजा · |
| आस्थादर्शन |
|---|
| पुनर्जन्म · मोक्ष |
| कर्म · माया |
| दर्शन · धर्म |
| वेदान्त ·योग |
| शाकाहार · आयुर्वेद |
| युग · संस्कार |
| भक्ति {{हिन्दू दर्शन}} |
| ग्रन्थशास्त्र |
| वेदसंहिता · वेदांग |
| ब्राह्मणग्रन्थ · आरण्यक |
| उपनिषद् · श्रीमद्भगवद्गीता |
| रामायण · महाभारत |
| सूत्र · पुराण |
| शिक्षापत्री · वचनामृत |
| सम्बन्धित |
| विश्व में हिन्दू धर्म |
| गुरु · मन्दिर देवस्थान |
| यज्ञ · मन्त्र |
| शब्दकोष · हिन्दू पर्व |
| विग्रह |
| प्रवेशद्वार: हिन्दू धर्म |
|
|
| हिन्दू मापन प्रणाली |
आधुनिक हिन्दू धर्म इसी धार्मिक व्यवस्था पर आधारित हैं। वैदिक संस्कृत में लिखे चार वेद इसकी धार्मिक किताबें हैं। हिन्दू मान्यता के अनुसार ऋग्वेद और अन्य वेदों के मन्त्र ईश्वर द्वारा ऋषियों को प्रकट किये .गए थे। इसलिए वेदों को 'श्रुति' (यानि, 'जो सुना गया है') कहा जाता है, जबकि श्रुतिग्रन्थौके अनुशरण कर वेदज्ञद्वारा रचा गया वेदांगादि सूत्र ग्रन्थ स्मृति कहलाता है। वेदांग अन्तर्गत के धर्मसूत्र पर ही आधार करके वेदज्ञ मनु,अत्रि,याज्ञावल्क्य आदि द्वारा रचित अनुस्मतिृको भी स्मृति ही माना जाता है।ईसके वाद वेद-वेदांगौंके व्याखाके रुपमे पुराणखण्ड और रामायण-महाभारत रुपमे ईतिहासखण्ड को वेदव्यास और वाल्मीकि द्वारा रचा गया जिसके नीब पर वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म, विभिन्न वैष्णवादि मतसम्बद्ध हिन्दूधर्म ,और अर्वाचीन वैदिक मत आर्यसमाजी,आदि सभीका व्यवहार का आधार रहा है। कहा जाता है। वेदों को 'अपौरुषय' (यानि 'जीवपुरुषकृत नहीं') भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि उनकी कृति दिव्य है, अतःश्रुति मानवसम्बद्ध दोषमुक्त है। "प्राचीन वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म"का सारा धार्मिक व्यवहार विभन्न वेद शाखा सम्बद्ध कल्पसूत्र,श्रौतसूत्र,गृह्यसूत्र,धर्मसूत्र आदि ग्रन्थौंके आधारमे चलता है। इसके अलावा अर्वाचीन वैदिक (आर्य समाज) केवल वेदौंके संहिताखण्डको ही वेद स्वीकारते है।
वैदिक धर्म और सभ्यता की जड़ में सन्सारके सभी सभ्यता किसी न किसी रूपमे दिखाई देता है। आदिम हिन्द-अवेस्ता धर्म और उस से भी प्राचीन आदिम हिन्द-यूरोपीय धर्म तक पहुँचती हैं, जिनके कारण बहुत से वैदिक देवी-देवता यूरोप, मध्य एशिया/ईरान के प्राचीन धर्मों में भी किसी-न-किसी रूप में मान्य थे, जैसे ब्रह्मयज्ञमे जिनका आदर कीया जाता है उन ब्रह्मा,विष्णु,रुद्र,सविता,मित्र, वरुण,और बृहस्पति (द्यौस-पितृ), वायु-वात, सरस्वती,आदि। इसी तरह बहुत से वैदिकशब्दों के प्रभाव सजातीय शब्द अवेस्ताधर्म और प्राचीन यूरोपीय धर्मों में पाए जाते हैं, जैसे कि सोम (फ़ारसी: होम), यज्ञ (फ़ारसी: यस्न), पितर- फादर,मातर-मादर,भ्रातर-ब्रदर स्वासार-स्विष्टर नक्त-नाइट् इत्यादि। [1] यही इन् दोनो में वि/संगति है।
आत्मा की एकता
वैदिक धर्म में आत्मा की एकता पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। जो आदमी इस तत्व को समझ लेगा, वह किससे प्रेम नहीं करेगा? जो आदमी यह समझ जाएगा कि 'घट-घट में तोरा साँईं रमत हैं!' वह किस पर नाराज होगा? किसे मारेगा? किसे पीटेगा? किसे सताएगा? किसे गाली देगा? किसके साथ बुरा व्यवहार करेगा?
यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥
जो आदमी सब प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, उसके लिए किसका मोह, किसका शोक? वैदिक धर्म का मूल तत्व यही है। इस सारे जगत में ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त है। उसी को पाने के लिए, उसी को समझने के लिए हमें मनुष्य का यह जीवन मिला है। उसे पाने का जो रास्ता है, उसका नाम है धर्म।
धर्म के चार लक्षण मनु महाराज ने धर्म के चार लक्षण बताए हैं:
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम्॥
धर्म की कसौटी चार हैं :
- वेद,
- स्मृति,
- सदाचार तथा
- आत्मा को रुचने वाला आचरण
वेद
वेद चार हैं। हर वेद के चार विभाग हैं : संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् हिन्दू धर्म का मूल आधार है वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान। संस्कृत की 'विद्' धातु से 'वेद' शब्द बना है। 'विद्' यानी जानना।
वेद को 'श्रुति' भी कहा जाता है। 'श्रु' धातु से 'श्रुति' शब्द बना है। 'श्रु' यानी सुनना। कहते हैं कि ऋषियों को अंतरात्मा में परमात्मा के पास से आता ज्ञान सुनाई पड़ा।
वेद चार हैं : ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
- ऋग्वेद : यह सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं और 10627 मंत्र। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना और स्तुतियाँ हैं।
- यजुर्वेद : इसमें 1975 मंत्र और 40 अध्याय हैं। इस वेद में अधिकतर यज्ञ के मंत्र हैं।
- सामवेद : इसमें 1875 मंत्र हैं। ऋग्वेद की ही अधिकतर ऋचाएँ हैं। इस संहिता के सभी मंत्र संगीतमय अर्थात गेय हैं।
- अथर्ववेद : इसमें 5977 मंत्र और 20 कांड हैं। इसमें भी ऋग्वेद की बहुत-सी ऋचाएँ हैं।
चारों वेदों में कुल मिलाकर 20454 मंत्र हैं।
- वैदिक ऋषि
प्राचीनकाल में भारत देश में जो लोग ज्ञानी थे, आचार-विचार वाले थे, जिनका हृदय उदार था, जिनके विचार ऊँचे थे, उन्हें लोग 'ऋषि' कहा करते थे। 'सादा जीवन, उच्च विचार' उनका आदर्श था।
वे धर्म के गूढ़ विषयों पर चिंतन करते थे, सादा और पवित्र जीवन बिताते थे और समाज को सही रास्ता दिखाया करते थे। वैदिक साहित्य इन ऋषियों की ही पवित्र धरोहर है। 5000 साल पहले भी उससे लोगों को प्रेरणा मिलती थी और आज भी मिलती है।
- वैदिक देवता
वेदों में हमें बहुत से देवताओं की स्तुति और प्रार्थना के मंत्र मिलते हैं। इनमें मुख्य-मुख्य देवता ये हैं :
| वेदों के देवतागण |
|---|
कभी तो हम शरीर को मनुष्य कहते हैं, कभी उसकी आत्मा को। उसी तरह वैदिक ऋषि भी दो रूपों में देवताओं की प्रार्थना करते थे। कभी जड़ पदार्थ के रूप में, कभी उस जड़ के भीतर रहने वाले चेतन परंपरा के रूप में। जैसे- 'सूर्य' शब्द से कभी उनका आशय होता था उस तेज चमकते हुए गोले से, जिसे हम 'सूर्य' कहकर पुकारते हैं।
कभी 'सूर्य' से उनका आशय होता था, सूर्य के रूप में प्रकाशमान परमात्मा से। ऋषियों का ऐसा विश्वास था कि एक ही महान सत्ता नाना देवताओं के रूप में बिखरी है। उसी की वे स्तुति करते थे, उसी की प्रार्थना। उसी की वे उपासना करते थे। उसी को प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ करते थे।
मंत्रों का सौंदर्य
वेद के मंत्रों में सुंदरता भरी पड़ी है। वैदिक पंडित जब स्वर के साथ वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, तो चित्त प्रसन्न हो उठता है। जो भी सस्वर वेदपाठ सुनता है, मुग्ध हो उठता है।
इतना ही नहीं, ऋचाओं में जो अर्थ भरा है, वह तो उससे भी सुंदर है। उनमें जो भाव भरे हैं, वे मनुष्य को ऊपर उठाने वाले हैं। समाज को ऊपर उठाने वाले हैं। उनसे आत्मा का भी कल्याण होता है, समाज का भी।
कर्म, ज्ञान और उपासना
वेदों के मुख्य रूप से तीन भाग हैं : 1) कर्मकाण्ड, 2) ज्ञानकाण्ड और 3) उपासनाकाण्ड
कर्मकाण्ड में यज्ञ कर्म दिया गया है, जिससे यज्ञ करने और कराने वाले को लोक-परलोक में सुख मिले।
ज्ञानकाण्ड में परमात्मा और आत्मा का तत्व और लोक-परलोक का रहस्य बताया गया है।
उपासनाकाण्ड में ईश्वर-भजन की विधि बताई गई है। इससे मनुष्य को लोक-परलोक में सुख मिल सकता है और ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।
वेद के अंतर्गत चार विभाग हैं: 1) संहिता, 2) ब्राह्मण, 3) आरण्यक और 4) उपनिषद् |
वेदों के मूल पाठ को संहिता कहते हैं। यह चारों वेदों के अलग-अलग पाठ हैं।
चारों वेदों की कई शाखाएं हो चुकी हैं और उन सभी शाखाओं के अपने-अपने ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद रहे हैं जिनमें से अधिकाँश आजकल अनुपलब्ध हैं।
ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से यज्ञों की चर्चा है। इसमें वेदों के मंत्रों की व्याख्या के साथ-साथ यज्ञों के विधान का विस्तार से वर्णन है।
मुख्य ब्राह्मण 4 हैं :
- ऐतरेय,
- तैत्तिरीय,
- शतपथ तथा
- गोपथ|
- आरण्यक में कहा है
वेदों की रचना ऋषियों ने की है। वे रहते थे वनों में, जंगलों में। वन को संस्कृत में कहते हैं 'अरण्य'। अरण्यों में बने हुए ग्रंथों का नाम पड़ गया 'आरण्यक'।
मुख्य आरण्यक पाँच हैं :
- ऐतरेय,
- शांखायन,
- बृहदारण्यक,
- तैत्तिरीय और
- तवलकार।
उपनिषद
वेद के अंतिम भाग का नाम है उपनिषद्। उपनिषद् शब्द बना है सद् धातु से। सद् का अर्थ होता है नाश होना, और शिथिल हो जाना। उपनिषद् का अर्थ है ब्रह्मविद्या। ब्रह्मविद्या से अविद्या का नाश होता है, जगत के बंधन शिथिल हो जाते हैं, आनंद मिलता है और जन्म-मरण का दुःख छूट जाता है।
- मुख्य उपनिषद्
सभी वेदों की अपनी-अपनी सभी शाखासम्बद्ध उपनिषदें होती हैं। आजकल 108 उपनिषदें मिलती हैं। जिसमे आचार्य शंकर लगायत विद्वानके भाष्य मिलते ऐसे मुख्य उपनिषदें १० हैं- ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वरको भी प्रमुख मानाजाता है।
स्मृति
- मुख्य स्मृतियाँ हैं
- मनु स्मृति (मानव धर्मशास्त्र),
- याज्ञवल्क्य स्मृति,
- अत्रि स्मृति,
- विष्णु स्मृति,
- आपस्तम्ब स्मृति,
- पाराशर स्मृति,
- व्यास स्मृति और
- वशिष्ठ स्मृति।
दीक्षा और तप
सत्य की साधना के लिए दीक्षा भी चाहिए और तपस्या भी।
यजुर्वेद में कहा है :-
व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्ध्या सत्यमाप्यते॥
व्रत से दीक्षा मिलती है, दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा से श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है।
तप का अर्थ
इंद्रियों का संयम। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तप करना ही पड़ता है। धर्म को पाने के लिए भी तप करना जरूरी है। ब्रह्मचर्य-जीवन में जिस तरह तपस्या करनी पड़ती है, उसी तरह आगे भी।
ब्रह्मयज्ञ
ब्रह्मयज्ञका अर्थ है गुरुमुखसे अनुवचन कीया हुआ वेद-श्रुति (मन्त्रब्राह्मणात्मक) वेदभागको नित्य विधिवत् पाठ करना। पाठमे असमर्थसे वैदिक मंत्रोंका जप करना भी अनुकल्प विधिसे ब्रह्मयज्ञ ही है। ब्राह्मण वेदोंके जिस् यज्ञ-अनुष्ठानका प्रसंगवाला भाग नित्य पाठ करता है उसी यज्ञका फल प्राप्त करता है। प्राचीन कालमे जिसने वेदानुवचन कीया है वह प्रतिदिन शुक्लपक्षमे मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदभाग और कृष्णपक्षमे वेदांग-कल्प,व्याकरण,निरुक्त,शिक्षा,छन्द और ज्योतिष पाठ करता था। प्रार्थना और यज्ञसे सम्बन्ध रख्नेवाला यजमान और पुरोहित- ऋत्विक् वा आचार्य सदाचारी(वेदोक्त वर्णाश्रमधर्मका पालक)होना चाहिए। नहीं तो उसकी पूजा-प्रार्थना वा यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है। पुराणौंमे कहा भी है- आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीता सहषड्भिरंगैः ....| सदाचारी लोग ही तरते हैं, दुराचारी नहीं।
ऋग्वेद में कहा है :-
ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः।
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- The Rig-Veda and Vedic Religion, Forgotten Books, ISBN 978-1-4400-8579-6