ईशावास्य उपनिषद्
ईशोपनिषद् शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के अन्तर्गत एक उपनिषद है। यह उपनिषद् अपने नन्हें कलेवर के कारण अन्य उपनिषदों के बीच बेहद महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें कोई कथा-कहानी नहीं है केवल आत्म वर्णन है। इस उपनिषद् के पहले श्लोक ‘‘ईशावास्यमिदंसर्वंयत्किंच जगत्यां-जगत…’’ से लेकर अठारहवें श्लोक ‘‘अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विध्वानि देव वयुनानि विद्वान्…’’ तक शब्द-शब्द में मानों ब्रह्म-वर्णन, उपासना, प्रार्थना आदि झंकृत है। एक ही स्वर है — ब्रह्म का, ज्ञान का, आत्म-ज्ञान का।
| ईशावास्य उपनिषद् | |
|---|---|
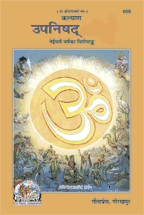 | |
| लेखक | वेदव्यास |
| चित्र रचनाकार | अन्य पौराणिक ऋषि |
| देश | भारत |
| भाषा | संस्कृत |
| श्रृंखला | शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद |
| विषय | ज्ञान योग, द्वैत अद्वैत सिद्धान्त |
| प्रकार | हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ |
परिचय
अद्भुत कलेवर वाले इस उपनिषद् में ईश्वर के सर्वनिर्माता होने की बात है सारे ब्रह्मांड के मालिक को इंगित किया गया है, सात्विक जीवनशैली की बात कही गई है कि दूसरे के धन पर दृष्टि मत डालो।
इस जगत् में रहते हुए निःसंङगभाव से जीवनयापन करने को बताया गया है। इसमें ‘असुर्या’ नामक लोक की बात आती है — असुर्या मतलब कि सूर्य से रहित लोक। वह लोक जहाँ सूर्य नहीं पहुँच पाता, घने, काले अंधकार से भरा हुआ अन्चतम लोक, अर्थात् गर्भलोक।
कहा गया है कि जो लोग आत्म को, अपने ‘स्व’ को नहीं पहचानते हैं, आत्मा को झुठला देते हैं, नकार देते हैं और इसी अस्वीकार तले पूरा जीवन बिताते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात् उसी अन्धतम लोक यानि कि असुर्या नामक लोक में जाना पड़ता है अर्थात् गर्भवास करना पड़ता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है।
इस प्रकार इस उपनिषद् में एक ओर ईश्वर को सर्वनिर्माता मानकर स्वयं को निमित्त मात्र बनकर जीवन जीने का इशारा करता है, जो दूसरी ओर आत्म को न भूलने की इंगित करता है।
इसके बाद आत्म को निरुपित करने का तथ्य आता है कि ‘वह’ अचल है साथ ही मन से भी ज्यादा तीव्रगामी है। यह आत्म (ब्रह्म) सभी इंद्रियों से तेज भागने वाला है।
इस उपनिषद् में आत्म/ब्रह्म को 'मातरिज्वा' नाम से इंगित किया गया है, जो कि सभी कार्यकलापों को वहन करने वाला, उन्हें सम्बल देने वाला है।
‘आत्म’ के ब्रह्म के गुणों को बताने के क्रम में यहाँ यह बताया गया है कि वह एक साथ, एक ही समय में भ्रमणशील है, साथ ही अभ्रमणशील भी। वह पास है और दूर भी। यहाँ उसे कई विशेंषणों द्वारा इंगित किया गया है — कि वह सर्वव्यापी, अशरीरी, सर्वज्ञ, स्वजन्मा और मन का शासक है।
इस उपनिषद् में विद्या एवं अविद्या दोनों की बात की गई है उनके अलग-अलग किस्म के गुणों को बताया गया है साथ ही विद्या एवं अविद्या दोनों की उपासना को वर्जित किया गया है — यहाँ यह साफ-साफ कहा गया है कि विद्या एवं अविद्या दोनों की (या एक की मा) उपासना करने वाले घने अंधकार में जाकर गिरते हैं साकार की प्रकृति की उपासना को भी यहाँ वर्जित माना गया है लेकिन हाँ विद्या एवं अविद्या को एक साथ जान लेने वाला, अविद्या को समझकर विद्या द्वारा अनुष्ठानित होकर मृत्यु को पार कर लेता है, वह मृत्यु को जीतकर अमृतत्व का उपभोग करता है यह स्वीकारोक्ति यहाँ है।
इसमें सम्भूति एवं नाशवान् दोनों को भलीभाँति समझ कर अविनाशी तत्व प्राप्ति एवं अमृत तत्व के उपभोग की बात कही गई है। इस उपनिषद् के अंतिम श्लोकों में बड़े ही सुंदर उपमान आते हैं — ब्रह्म के मुख को सुवर्ण पात्र से टंके होने की बात साथ ही सूर्य से पोषण करने वाले से प्रार्थना की। सुवर्णपात्र से टंके हुए उस आत्म के मुख को अनावृत कर दिया जाए ताकि उपासक समझ सके, महसूस कर सके कवह स्वयं ही ब्रह्मरूप है और अंतिम श्लोकों में किए गए सभी कर्मों को मन के द्वारा याद किए जाने की बात आती है और अग्नि से प्रार्थना कि पंञचभौतिक शरीर के राख में परिवर्तित हो जाने पर वह उसे दिव्य पथ से चरम गंतव्य की ओर उन्मुख कर दे।
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
मूल ग्रन्थ
अनुवाद
- Translations of major Upanishads
- 11 principal Upanishads with translations
- Translations of principal Upanishads at sankaracharya.org
- Upanishads and other Vedanta texts
- डॉ मृदुल कीर्ति द्वारा उपनिषदों का हिन्दी काव्य रूपान्तरण
- Complete translation on-line into English of all 108 Upaniṣad-s [not only the 11 (or so) major ones to which the foregoing links are meagerly restricted]-- lacking, however, diacritical marks